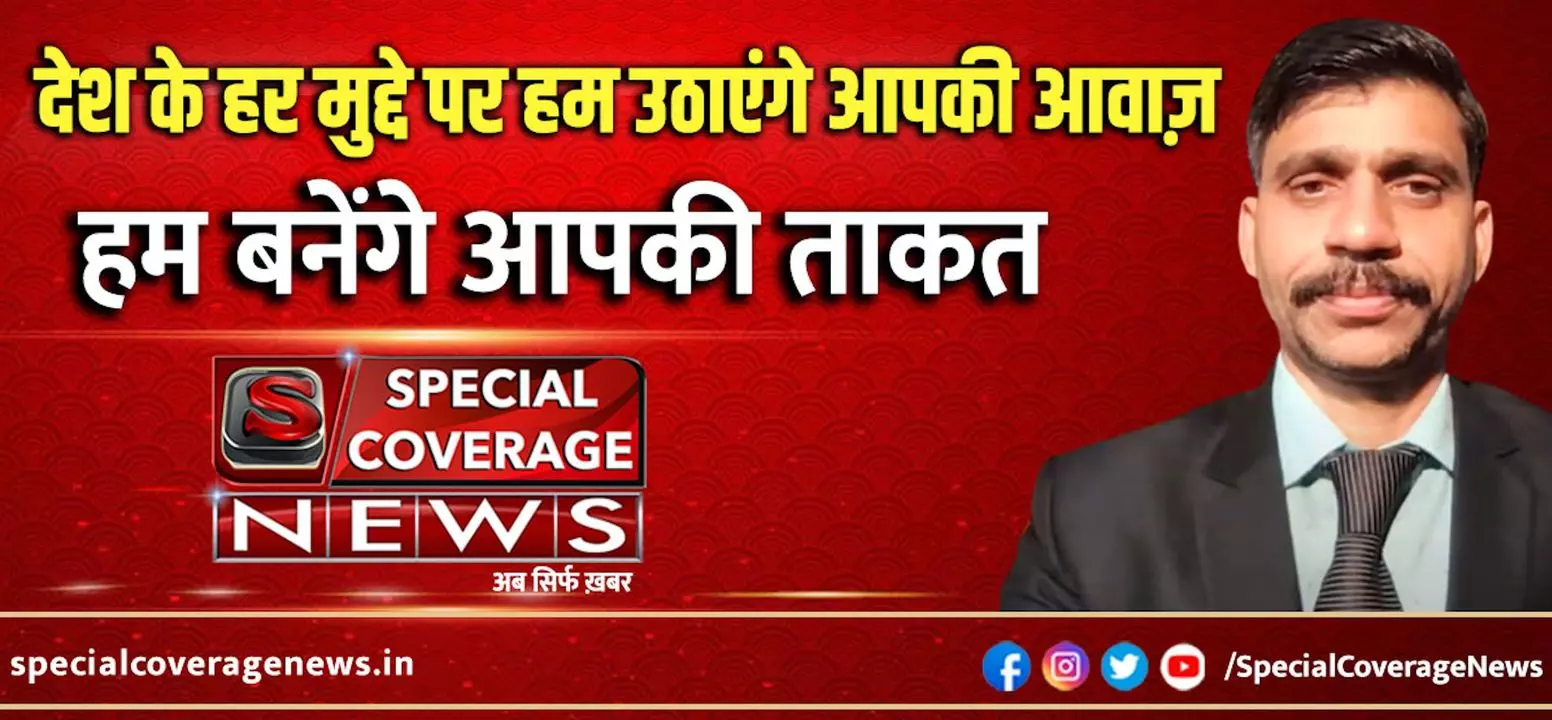- Home
- /
- हमसे जुड़ें
- /
- कांग्रेस और संघ का...

पी. चिदंबरम का साप्ताहिक कॉलम
एक वक्त था जब कोई विचार या विचारधारा एक मजबूत बंधन बन जाती थी, जो विभिन्न राज्यों के, भिन्न भाषाएं बोलने वालों को, अलग-अलग आस्था रखने वालों को, अलग-अलग जातियों में जन्मे लोगों और समाज के अलग-अलग आर्थिक वर्गों के लोगों को एक साथ ले आती थी। इस विचार या विचारधारा के आधार पर ही राजनीतिक दलों की स्थापना हुई। भारत में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी।
कांग्रेस के संस्थापकों का असल मकसद शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में ज्यादा भागीदारी हासिल करना और उनके व ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद के लिए एक मंच तैयार करना था। आजादी हासिल करने का कोई विचार नहीं था।
यह बहुत बाद में 1919 से 1929 के बीच आया था। दूसरा उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) है। हालांकि यह कहता है कि यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसके सदस्य हिंदू राष्ट्र के विचार से बंधे हैं। शुरुआती वर्षों में इसका मतलब जो रहा हो, इस वक्त तो यह संज्ञाहीन व विद्वेष फैलाने वाली विचारधारा बन गई है जो मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, अप्रवासियों को दबे-छिपे तरीके से निशाना बनाती है और महिलाओं, गैर-हिंदीभाषी लोगों और अन्या पिछड़े वर्गों की उपेक्षा करती है।
राज्यों के स्तर पर बहुत से उदाहरण हैं। डीएमके की स्थापना क्षेत्रीय अस्मिता, तमिल प्रेम, आत्मसम्मान, अंधविश्वास विरोध और जाति विरोध के आधार पर हुई थी। इसकी विभाजक एआइएडीमके का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष से हुआ था।
उभरती विचारधाराएं
कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं, जो बदली न हो। बाद के वर्षों में कांग्रेस ने आजादी हासिल करने की प्रतिज्ञा की और परंपरावादियों और प्रगतिशीलों को साथ लिया, वाम की तरफ रुझान बढ़ा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को स्वीकार किया और केंद्र में पहुंची, बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, कल्याणवाद को अंगीकार किया, और अब अपनी आर्थिक व सामाजिक नीतियों को परिभाषित करने की कोशिश कर रही है जो इसे भाजपा से अलग करेंगी। भाजपा निश्चित रूप से और ज्यादा हिंदू राष्ट्रवादी व ज्यादा पूंजीवादी बन गई है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है। क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी नीतियों और स्थितियों में थोड़ा बदलाव किया है। उदाहरण के लिए एआइएडीएमके जो डीएमके से टूट कर अलग हुई थी, शुरुआत से ही ईश्वरवादी पार्टी थी और हाल के वर्षों में डीएमके ने अनीश्वरवादी होने का चोला ओढ़ लिया है।
मैंने इन दलों और बदलती विचारधाराओं पर चर्चा की है। हर विचारधारा अपने समर्थकों को शामिल करती लगती है, लेकिन अपने में आस्था नहीं रखने वालों को अलग कर देती है, जिनका वोट और समर्थन भी उतना ही जरूरी होता है, जितना कि उसमें आस्था रखने वालों का। इसलिए उसमें सतत बदलाव और सामंजस्य की जरूरत होती है। उसे नहीं मानने वाले जो अपने को उससे बाहर पाते हैं, नई राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं जो उनकी सहानुभूति या विद्वेष को प्रतिबिंबित करती है। इस प्रकार के खास विरोध से ही कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर), जनता दल, समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), बीजू जनता दल और तेलुगु देशम जैसी पार्टियां बनीं। अलग राज्य या ज्यादा स्वायत्तता की मांग से प्रेरित होकर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और असम गण परिषद (एजीपी) बनी थी।
निष्कासन की राजनीति
भारत में तमाम राजनीतिक दलों ने लोगों के महत्त्वपूर्ण वर्गों को छोड़ दिया था या वे अपने को अलग हुआ महसूस कर रहे थे और अब भी उन्हें ऐसा ही लग रहा है। इनमें मुसलमान और दलित भी हैं। इन वर्गों को सांप्रदायिक या जातिवादी समझ कर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इन्हें मुख्यधारा की राजनीति से बाहर किया गया तो फिर ये वर्ग अपने राजनीतिक दल बनाना शुरू कर देंगे, जो उचित भी है। मेरे विचार से ऐसा बहिष्कार, या तो कानूनी तौर पर या वास्तविक, भारतीय राजनीति और गठबंधनों की इच्छा को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।
मुझे याद पड़ता है कि 2017 में गुजरात या उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक भी मुसलिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। गुजरात में मुसलिम आबादी 9.65 फीसद है और एक सौ बयासी विधानसभा सीटें, जबकि उत्तर प्रदेश में चार सौ दो सीटें और 19.3 फीसद मुसलिम आबादी। इन दो राज्यों में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? दूसरे दलों ने वास्तव में अलग दृष्टिकोण अपनाया, मुसलिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन यह भी दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं था। दलितों के मामले में सभी दलों ने उन्हें आरक्षित सीटों तक सीमित कर दिया। इसका नतीजा राजनीतिक समावेशन से ज्यादा राजनीतिक निष्कासन रूप में सामने आया। समय के साथ मुसलमान, दलित और दूसरे बहिष्कृत वर्गों ने अपने हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अलग पार्टियां बनाने की जरूरत को महसूस किया।
आल इंडिया मुसलिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आजाद भारत में मुसलिमों द्वारा बनाई गई कई पार्टियां हैं- आइयूएमएल, एआइयूडीएफ, एआइएमआइएम और कई अन्य छोटी पार्टियां। इसी तरह दलितों ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा), लोक जनशक्ति पार्टी (बिहार में) और तमिलनाडु में वीसीके (विदुथालाई चिरुथैगल काच्चि) बनाई थी। आरएसएस और भाजपा ने मुसलिमों द्वारा बनाई पार्टियों को रगड़ा, लेकिन दलित पार्टियों के साथ गठजोड़ कर लिए, इससे ज्यादा स्वार्थी होने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। (असम में जिला परिषद के चुनावों में भाजपा ने एआइयूडीएफ के साथ समझौता किया था।)
शासन के लिए बेहतर
समाज के भिन्न वर्गों को छोड़ कर राजनीति करने वाले दलों की संख्या के मुकाबले गठजोड़ करने वालों ने ज्यादा समावेशी राजनीति का रास्ता दिखाया है। मौजूदा चुनावों में मुसलिमों और दलितों की पार्टियों ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में गठजोड़ करके अपनी जगह बनाई है। मेरे विचार से यह अच्छा है। अगर ये पार्टियां अकेले लड़ीं तो विधायी निकायों में प्रवेश इनके लिए मुश्किल हो जाएगा और ये तमाशबीन और आंदोलनकारी बनने को मजबूर हो जाएंगी। बेहतर यह है कि ये संसद और राज्य विधानसभाओं में पहुंचें और देश व राज्यों के शासन में भागीदार बनें।
हर पार्टी गठजोड़ को बनाए रखने की कोशिश करती है। यह संभव है कि कुछ राज्यों में कुछ चुनावों में कोई दल अपने बूते बहुमत हासिल करने में कामयाब हो जाए, तब भी ऐसे मामलों में वह पार्टी कुछ और दलों को अपने साथ रखने को प्राथमिकता देना चाहेगी, ताकि उसका बहुमत और सशक्त बन जाए। ज्यादातर चुनाव अब गठजोड़ों के बीच चुनाव हो गए हैं। हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में दो मुख्य गठबंधन एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में तीन गठबंधन हैं, लेकिन सबकी ताकत अलग-अलग है। मेरा अनुभव यह बताता है कि गठबंधन की सरकार ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा उत्तरदायी होती है।
वाजपेयी जी और डा. मनमोहन सिंह की सरकारें गठबंधन सरकारें थीं। इसलिए हमें चुनावी गठबंधनों या गठबंधन सरकारों को कोसना नहीं चाहिए। ऐसी सरकारें एक दलीय स्वेच्छाचारी शासनों से बेहतर होती हैं और बेहतर नतीजे देती हैं।
[इंडियन एक्सप्रेस में 'अक्रॉस दि आइल' नाम से छपने वाला, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता, पी चिदंबरम का साप्ताहिक कॉलम। जनसत्ता में यह 'दूसरी नजर' नाम से छपता है। हिन्दी अनुवाद जनसत्ता से साभार। शीर्षक मेरा है।]
संजय कुमार सिंह